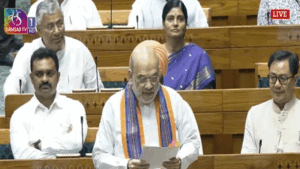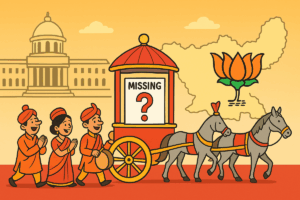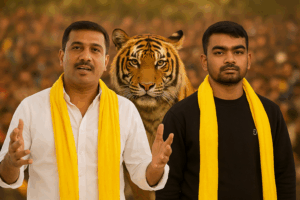ऑपरेशन सिंदूर’ और संघर्ष विराम पर ट्रंप बनाम मोदी: मध्यस्थता, रणनीति और भारत की चुनौती
प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के विरोधाभासी बयानों के बीच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर संघर्षविराम को लेकर उठे सवालों का विश्लेषण। क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में झुकाव दिखाया? वैश्विक मीडिया, मध्यस्थता और दक्षिण एशिया में परमाणु तनाव की पृष्ठभूमि में जानें भारत की रणनीतिक चुनौतियाँ।
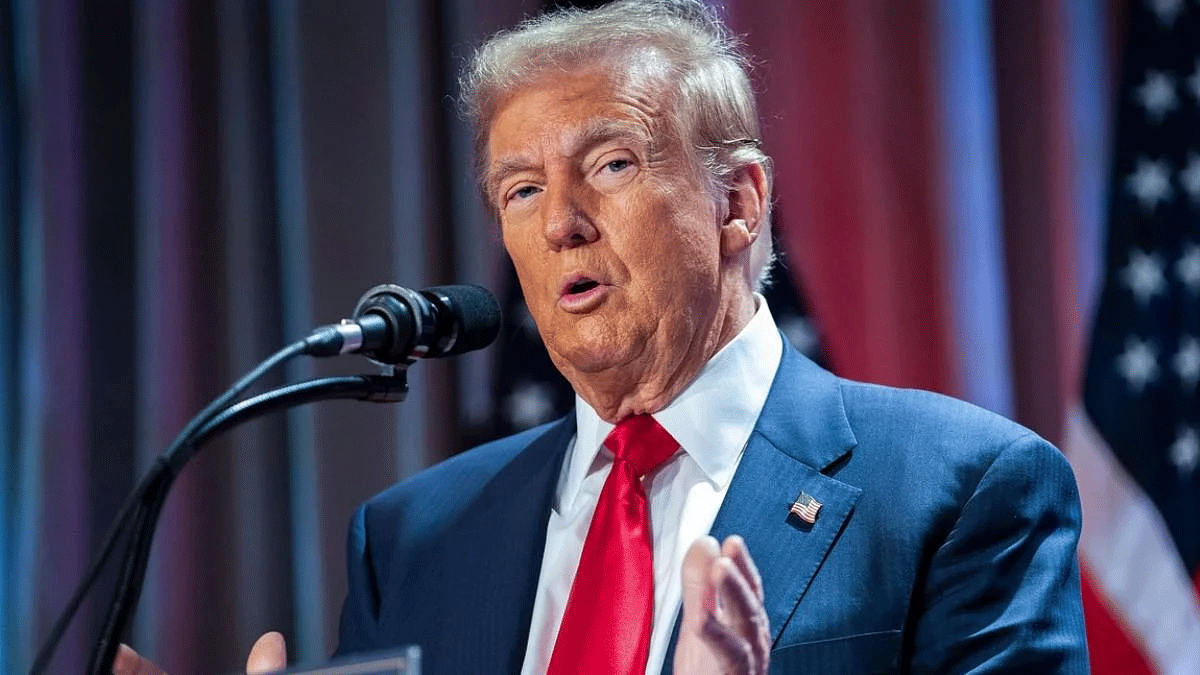

आनंद कुमार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2025 को राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में कहा कि पाकिस्तान के ‘सैन्य और आतंकी ठिकानों’ पर चलाया गया भारत का ऑपरेशन ‘सिंदूर’ फिलहाल “केवल स्थगित” किया गया है और आगे पाकिस्तान की हर हरकत इसी कसौटी पर जांची जाएगी। मोदी ने स्वयं कोई ‘संघर्ष-विराम’ शब्द प्रयोग नहीं किया और इसे एक द्विपक्षीय समझौता बताया। वहीं, उसी समय डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में कहा कि “हमने भारत-पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि यदि संघर्ष नहीं रुका तो व्यापार नहीं करेंगे” और इस दबाव के तहत ही दोनों पक्षों ने “पूर्ण और तत्काल युद्धविराम” स्वीकार कर लिया। ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि उनकी “व्यापार-आधारित कूटनीति” (trade as weapon) ने सम्भावित “भयानक परमाणु युद्ध” को टाल दिया। इन बयानों में परस्पर विरोध है। मोदी के संबोधन में पूरी छवि भारत की पहल और मजबूती की दिखती है, जबकि ट्रम्प के दावे में अमेरिका को ही संघर्ष विराम का पुरस्कर्ता बताया गया है। भारत सरकार ने ट्रम्प के दावे का जिक्र करने से बचते हुए इसे सिर्फ एक निजी राय माना है और युद्ध विराम को आपसी समझ बताया।
अमेरिका की कथित मध्यस्थता: दावे और यथार्थ
अमेरिकी दावों के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने संघर्षविराम वार्ता में सक्रिय भूमिका निभाई। रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया कि “चार दिनों की लड़ाई के बाद, अमेरिका के दबाव के बाद ही भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को संघर्षविराम पर सहमति व्यक्त की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार भी शांति अमेरिका की कूटनीति और दबाव के बाद बनी। ट्रम्प ने स्वयं कहा कि उनके प्रशासन ने “पूर्ण और तत्काल संघर्षविराम कराया” और व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी ओर, भारत में यह चर्चा उठी कि क्या भारत तीसरी पार्टी मध्यस्थता को स्वीकार कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने अलग से बयान नहीं दिया, लेकिन जीवंत आज तक ने बताया कि सरकार ने इसे सिर्फ “सैन्य कार्रवाई रोकने की द्विपक्षीय समझ” कहा और ‘संघर्षविराम’ शब्द का इस्तेमाल टाल दिया गया। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने भी नोट किया है कि ट्रम्प की घोषणाओं से कुछ भारतवासियों में यह भावना बनी कि मोदी सरकार अमेरिकी दबाव के सामने कुछ पीछे हट गई है तथा परंपरागत ‘तीसरे पक्ष की अस्वीकृति’ अछूती नहीं रही। कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री के चुप्पन पर सवाल उठाए और कहा कि यदि अमेरिका सचमुच मध्यस्थ रहा तो संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुल मिलाकर, वास्तविक स्थिति कुछ अस्पष्ट है: मीडिया और विदेशों में तो अमेरिका को “ब्रोकरेज” बताया गया, पर भारत की राजनैतिक पंक्तियों में इसे द्विपक्षीय पहल कहा जा रहा है।
वैश्विक मीडिया की प्रतिक्रियाएँ
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने संघर्षविराम को प्रमुखता से कवर किया, लेकिन कई जगहों पर अमेरिकी दृष्टिकोण को अग्रणी बताया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की लाइव अपडेट ब्लॉग में शीर्षक था “Trump announced Cease-Fire between India and Pakistan”, जबकि द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि “अमेरिका ने भारत-पाक संघर्षविराम दिलाने में मदद की, पर क्या यह टिक पाएगा?” न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी घोषणा को “US द्वारा मध्यस्थता की रातभर की वार्ता के बाद” बताया। अमेरिकी मीडिया स्रोत एनबीसी ने इसे साफ-साफ “US-brokered ceasefire” बताया और रॉलिंग स्टोन ने शीर्षक दिया “Trump takes credit for India, Pakistan cease-fire”। भारतीय मीडिया तथा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कई पश्चिमी आउटलेट्स की कवरेज में “ट्रम्प ने संघर्ष-विराम कराया” छाप हावी थी।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी लिखा कि संघर्षविराम अमेरिकी दबाव व कूटनीति के बाद बना, और ट्रम्प ने साथ ही कश्मीर पर “हजार सालों का समाधान” निकालने की पेशकश की। ब्रिटेन के गार्जियन ने परमाणु शक्ति के खतरों को रेखांकित करते हुए टिप्पणी की कि “जब दो परमाणु-शक्ति पड़ोसी आमने-सामने आ जाएं, तो हमें चिंता होनी चाहिए”। बीबीसी लंदन ने स्पष्ट किया कि “यूएस पहले ट्रम्प की घोषणा से पहले भारत-पाक समस्याओं से दूर था, लेकिन फिर हस्तक्षेप से संकट टला” जैसा शीर्षक। अल-जज़ीरा ने भी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि ट्रम्प प्रशासन ने संघर्ष विराम में भूमिका निभाई और ट्रम्प ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की। इसके अलावा, कुछ विश्लेषण आलेखों ने नोट किया कि अल-जज़ीरा में छपे एक ऑप-एड के अनुसार भारत की ‘दृष्टिकोण में कमी’ को देखकर यह लगा कि अमेरिका के दबाव में भारत ने झुकाव दिखाया। कुल मिलाकर वैश्विक मीडिया ने संघर्ष विराम को भारत-पाक के बीच की कहानी से हटकर “ट्रम्प की कूटनीति” की कहानी बना दिया, और यूएस की भागीदारी को लगातार आधार बनाकर दिखाया।
वैश्विक संस्थाओं और देशों की स्थिति
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत-पाक तत्काल संघर्षविराम की घोषणा का स्वागत किया और हतोत्साहित करने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करने का आश्वासन दिया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि हम संघर्ष को कम करने के हर प्रयास का स्वागत करते हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के देश अभी तक अग्रणी बयान नहीं दे पाए, लेकिन जी-7 और पाकिस्तान के करीबी देशों के स्तंभ जैसे ब्रिटेन ने भी संघर्षविराम को सराहा। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा: “आज का संघर्ष-विराम स्वागत योग्य है. मैं दोनों पक्षों से इसे बनाए रखने का आग्रह करता हूं. तनाव कम करना सभी के हित में है.”। रूस ने भी दोनों देशों को अपना करीबी बताया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने तनाव के बीच कहा कि रूस “नए दिलचस्प मुकाबलों” से गहरी चिंता में है और भारत-पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्तों को महत्व देता हैं। कुल मिलाकर, वैश्विक मंच से आम अपील शांति बनाए रखने और संवाद की रही है। विशेषकर यूएन ने संघर्षविराम का स्वागत किया, जबकि रूस, यूरोप और एशियाई देशों ने स्थिति पर कड़ी निगरानी की है।
नीतिगत परिप्रेक्ष्य: तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप और दबाव-आधारित कूटनीति
भारत की द्विपक्षीय कूटनीति की परंपरा में किसी भी बाहरी मध्यस्थता का विरोध सैद्धांतिक रूप से गहरा है। कश्मीर सहित सभी मसलों को सीधे बातचीत से हल करने के रुख पर भारत अडिग रहा है। ट्रम्प की बयानबाजी ने इस नीति को चुनौती दी है कि क्या भारत ने औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। सरकार ने इसका सीधे खंडन नहीं किया, पर मोदी जी के सम्बोधन में भी इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि कश्मीर पर कोई तीसरा पक्ष नहीं हो सकता – अब इसी बयान को धार देने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, ट्रम्प की ‘दबाव-आधारित कूटनीति’ ने यह दिखाया कि व्यापार वार्ता या प्रतिबंधों को हथियार बनाकर असंतुष्ट देशों को झुकाया जा सकता है। ट्रम्प ने साफ कहा: “हम आप लोगों से बहुत ज्यादा व्यापार करने जा रहे हैं… अगर आप झगड़ा बंद करते हो, तो हम व्यापार करेंगे; अगर नहीं करोगे, तो कोई व्यापार नहीं होगा.”। इस रणनीति में आर्थिक हितों को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ा गया है। भारत के सामने चुनौती यह है कि उसे अपने दम पर क्षेत्रीय विवाद सुलझाने का दावा कायम रखना है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक स्थितिजन्य दबाव को संभालना है। साथ ही, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते तेज करने की मजबूरी के बीच देशों पर कूटनीतिक दबाव नया आयाम जोड़ती है।
दक्षिण एशिया में परमाणु तनाव की पृष्ठभूमि
भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए इन खतरनाक टकरावों का हमेशा वैश्विक स्तर पर विशेष ध्यान रहा है। ट्रम्प और कई मीडिया ने खुलेआम कहा कि उन्होंने “परमाणु जंग रोकी”. गार्जियन ने लिखाः “जब दो परमाणु-शक्ति पड़ोसी आमने-सामने हों, तब स्थिति चिंताजनक है”। दक्षिण एशिया में लगातार संघर्षविराम की स्थिति अत्यधिक अस्थिर रही है; पिछले वर्ष ही अक्साई चीन जैसी जगहों पर भी तनाव दिखाई दिया। ऐसे में परमाणु दहनशीलता की आशंका बनी रहती है। संघर्षविराम के तुरंत बाद भी बॉर्डर पर गोलाबारी हुई और दोनों पक्षों ने सीमा पार दुश्मनी की बातें कीं, जिससे यह साफ है कि मौजूदा समझ अभी भी नाजुक है। इन सबके बीच भारत के लिए चुनौती है कि वह अपने परमाणु निवारक बल (डिटेरेंस) को अक्षुण्ण रखते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाए और वैश्विक स्तर पर यह आभास न होने दे कि जंग रुकी नहीं रही।
भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां
इस समूचे विश्लेषण से स्पष्ट है कि संघर्षविराम के बहाने भारत को कई रणनीतिक मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। पहला, भारत की कश्मीर पर परंपरागत ‘तीसरे पक्ष की मध्यस्थता’ से इनकार की नीति की सार्वभौमिक मान्यता वैसी नहीं रही – वैश्विक खिलाड़ी इसे ढीला पड़ते देख रहे हैं। दूसरे, अमेरिका की दबाव-आधारित सामरिक ताकत ने दिखाया कि आर्थिक विषयों को भी सुरक्षा कवायद से जोड़ा जा सकता है, जिससे भारत को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और लाभ के बीच समीकरण फिर से संतुलित करना है। तीसरा, वैश्विक मीडिया ने अक्सर भारत और पाकिस्तान की परस्पर द्वंद्व नहीं, बल्कि ट्रम्प की भुमिका को प्रमुखता दी, जिससे भारत की छवि और संदेश को पुनः संयोजित करने की आवश्यकता है। चौथा, परमाणु तनाव की पृष्ठभूमि में एक भी छोटी सी चूक भी भारी महंगी हो सकती है – इसलिए सीमाओं पर नियंत्रण बनाए रखना और कूटनीतिक रूप से दबाव घटाने के प्रयास अनिवार्य हैं। अंततः, भारत को अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ सीधी वार्ता की परंपरा को कायम रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वयं की विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारों के साथ सहयोग से राष्ट्रीय हित मजबूती से आगे बढ़ें। इन चुनौतियों का सार यही है कि भविष्य में भारत को न केवल सीमा सुरक्षा बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी गहरी समझदारी और लचीलापन दिखाना होगा, ताकि दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति की दिशा में मार्ग प्रशस्त हो सके।
स्रोत: वैश्विक मीडिया रिपोर्ट, सरकारी बयान, समाचार विश्लेषण एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर आधारित गहन अध्ययन