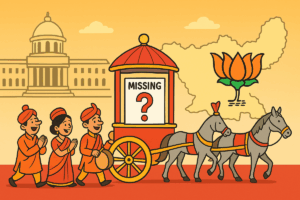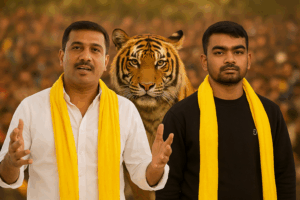जातीय गणना अक्टूबर 2026 से : पहले फेज में हिमाचल, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में, बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से
भारत में 1931 के बाद पहली बार 2026-27 में होगी आधिकारिक जातीय जनगणना। जानिए इसका इतिहास, राजनीतिक प्रभाव, और सामाजिक ताना-बाना कैसे बदलेगा।
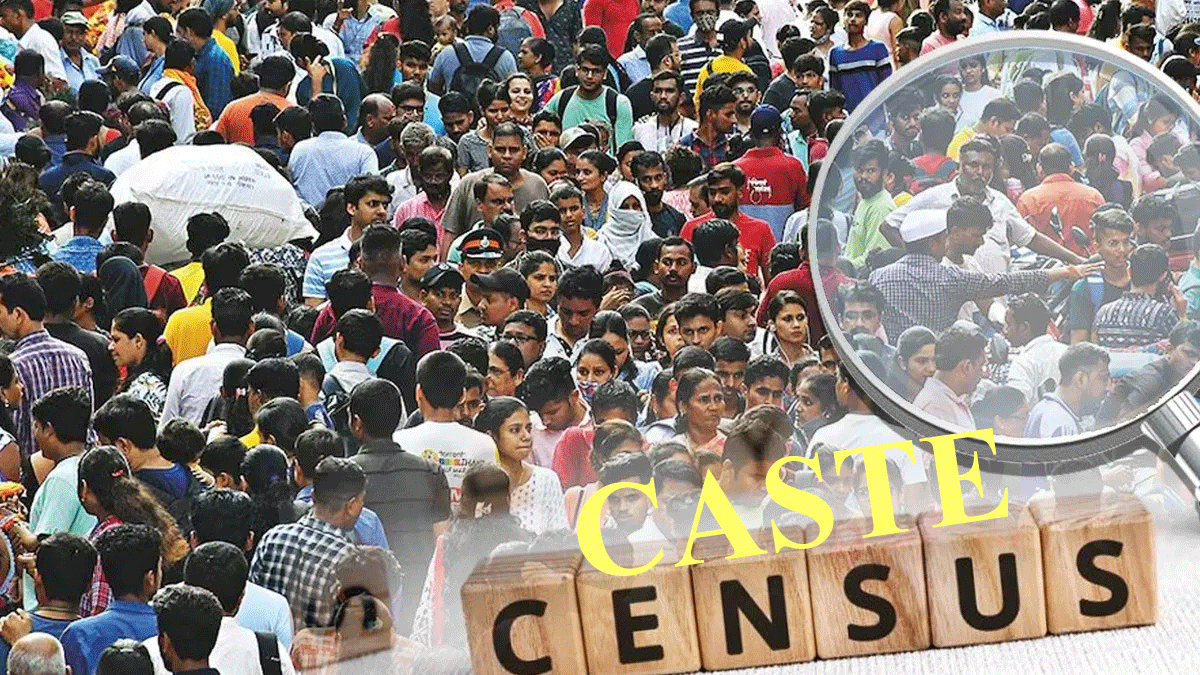
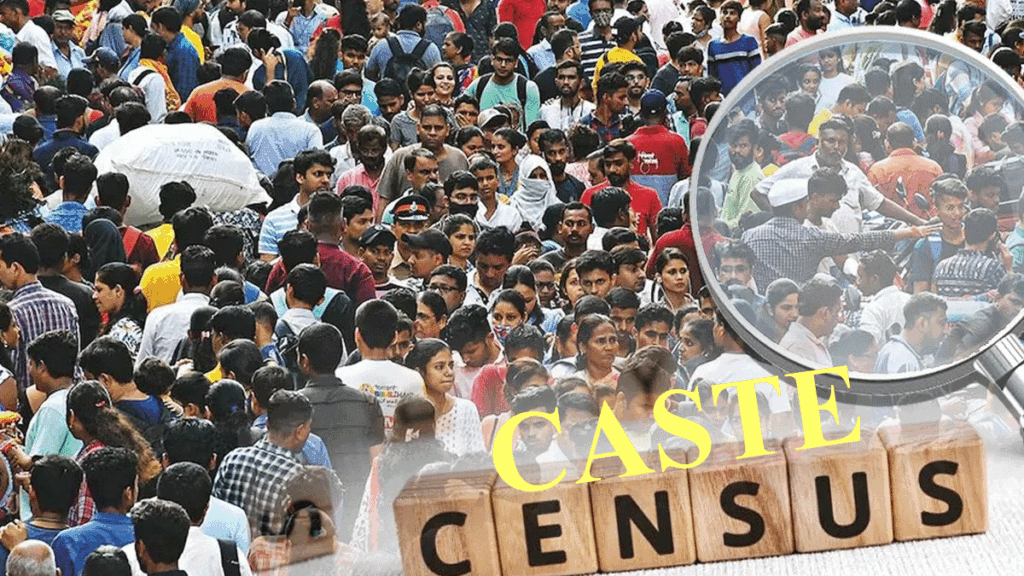
New Delhi – भारत की राजनीति और सामाजिक ढांचे में एक ऐतिहासिक मोड़ आता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि जातीय जनगणना अब दो चरणों में कराई जाएगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह स्पष्ट किया कि पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे चार पहाड़ी राज्यों को शामिल किया जाएगा। जबकि दूसरा और बड़ा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें देश के शेष राज्य शामिल होंगे।
यह केवल जनसंख्या गिनती भर नहीं होगी — सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसमें जातियों की गणना भी समानांतर रूप से की जाएगी, जो आजादी के बाद देश की पहली आधिकारिक जातीय जनगणना होगी।
देश में 1931 के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातिवार लोगों की गिनती होगी, लेकिन यह कब तक होगी, इसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है.
भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास एक लंबी चुप्पी से भरा हुआ है। आखिरी बार देश में जातियों की औपचारिक गिनती 1931 में हुई थी, और तब से अब तक 94 साल बीत चुके हैं। इस दौरान देश ने 17 बार जनगणना कराई, लेकिन हर बार जातियों को आंकड़ों से बाहर रखा गया — खासकर ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को।
इसका पहला संकेत आज़ादी के तुरंत बाद मिला, जब 1951 में संसद में जातीय जनगणना पर पहली अनौपचारिक चर्चा हुई। दिलचस्प यह है कि उस समय सभी राजनीतिक विचारधाराओं ने जातिगत गणना का विरोध किया। तर्क था कि यह सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकती है और जातिवाद को संस्थागत बना देगी। भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना, लेकिन जाति एक संवेदनशील मुद्दा बनकर रह गई। 1951 के बाद से हर जनगणना में केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और धार्मिक अल्पसंख्यकों की ही गिनती होती रही। ओबीसी (OBC) और जनरल कैटेगरी को आंकड़ों में शामिल ही नहीं किया गया।
भारत में जातिगत जनगणना को लेकर उठता हर सवाल हमें इतिहास की धूल लगी फाइलों की ओर ले जाता है, जहां 1941 की जनगणना एक अधूरी दस्तावेज़ बनकर रह गई है। यह वह जनगणना थी जो जाति के आधार पर विस्तृत आंकड़े जुटाने के इरादे से की गई थी, लेकिन इसके परिणाम कभी देश की नजरों के सामने नहीं आ सके।
⚔️ धर्म बनाम जाति: राजनीतिक खींचतान की जड़ें
द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तब 1941 की जनगणना के जरिए जातियों की गणना की योजना बनाई गई थी। लेकिन जनगणना के दौरान मुस्लिम लीग ने अपने समुदाय से “जाति” की जगह “इस्लाम” लिखवाने पर ज़ोर दिया। उनका तर्क था कि मुस्लिम समाज जातियों में विभाजित नहीं है और उन्हें एकसाथ इस्लामिक पहचान के तहत ही देखा जाए।
वहीं दूसरी ओर, हिंदू महासभा ने भी हिंदुओं से आग्रह किया कि वे जाति के बजाय केवल “हिंदू” धर्म लिखवाएं, ताकि हिंदू समाज एकजुट दिखाई दे।
यह विचारधारा टकराव की स्थिति में तब्दील हो गई। जब दो प्रमुख राजनैतिक ध्रुव जाति को दरकिनार कर धर्म की पहचान को प्राथमिकता देने लगे, तब जनगणना के वास्तविक उद्देश्य पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया।
📦 अंक नहीं, विवाद मिला — और फिर चुप्पी
1941 की जनगणना तो हो गई, लेकिन इन विवादों और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के चलते इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। ब्रिटिश सरकार ने इसे एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय मानते हुए दबा दिया।
इस तरह भारत की जातिगत संरचना का महत्वपूर्ण डेटा इतिहास के अंधेरे में खो गया।
🔥 1947: धार्मिक विभाजन और नई गणना नीति
1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, वह केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी — वह एक धार्मिक विभाजन की पीड़ा भी साथ लेकर आया था।
देश के दो टुकड़े हुए — भारत और पाकिस्तान — और बंटवारे की नींव धर्म के आधार पर रखी गई थी।
ऐसे माहौल में नई सरकार ने तय किया कि जातिगत आधार पर कोई जनगणना नहीं होगी, ताकि धार्मिक बंटवारे के बाद अब सामाजिक बंटवारा न हो।
यह नीति 1951 की पहली स्वतंत्र भारत की जनगणना से लागू हुई, जिसमें एससी, एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के आंकड़े तो लिए गए, लेकिन जातियों की गिनती नहीं की गई।
🛑 कांग्रेस की प्रतिक्रिया और जाति पर प्रतिबंध
जब देशभर में जातियों की गिनती की मांग उठी, तो कांग्रेस पार्टी ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। उस समय की पार्टी लाइन यह थी कि “जातिगत गणना ब्रिटिश सरकार का समाज तोड़ने वाला षड्यंत्र” था।
और इस तरह जातिगत आंकड़ों पर लगा पर्दा आज तक पूरी तरह नहीं हट सका।
🔁 इतिहास का पुनरावलोकन: 2011 और उसके बाद की चुप्पी
जातीय जनगणना की मांग कोई नई नहीं है। 2011 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए। केवल SC-ST हाउसहोल्ड के आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मोदी सरकार ने जून 2014 में संसद को बताया कि SECC पूरा होने में 3 महीने और लगेंगे, लेकिन आंकड़े कभी जारी नहीं किए गए।
2018 में सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया कि डेटा प्रोसेसिंग में कई तकनीकी गड़बड़ियां मिली हैं।
जनगणना अधिनियम 1948 केवल SC-ST की गणना का प्रावधान देता है। OBC की गणना के लिए अधिनियम में संशोधन आवश्यक होगा, जिससे देश की लगभग 2,650 पिछड़ी जातियों के आंकड़े सामने आ सकते हैं।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट में सरकार का रुख: “मुश्किल और जटिल”
2021 में, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट किया कि एससी-एसटी के अलावा अन्य जातियों की गिनती प्रशासनिक रूप से मुश्किल है।
इसके बाद गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि सरकार फिलहाल किसी अन्य जाति की गणना नहीं कराएगी। यह साफ संकेत था कि सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ है।
🔥 राजनीतिक दबाव और विपक्ष की रणनीति
लेकिन राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती।
कांग्रेस, सत्ता से बाहर होते ही, जातिगत जनगणना को जनाधार की राजनीति से जोड़ने लगी।
राहुल गांधी, जिन्होंने इसे दलितों और ओबीसी समुदाय के हक का सवाल बना दिया, लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे।
इस मुहिम में सपा, बसपा, आरजेडी, डीएमके, भाकपा(माले) जैसे दल भी शामिल हो गए और देश भर में एक ‘जाति आधारित अधिकार’ का नैरेटिव खड़ा किया गया।
🧾 राज्यों की चाल: कास्ट सर्वे के नाम पर जनगणना
हालांकि संविधान का अनुच्छेद 246 स्पष्ट करता है कि जनगणना केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य सरकारों ने “कास्ट सर्वे” के नाम से इस प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू कर दिया।
- बिहार की नीतीश सरकार ने 2023 में जातिगत सर्वे कराया और सार्वजनिक किया।
- कर्नाटक में 2015 में सिद्धारमैया सरकार ने कास्ट सर्वे किया।
- तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने भी 2023 में एक सामाजिक-आर्थिक और जातिगत सर्वे कराया।
इन सब प्रयासों ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया।
🧠 संघ का रुख बदला, और बदल गई सरकार की सोच
जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातिगत जनगणना को लेकर लचीला रुख दिखाना शुरू किया, तो राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई कि सरकार भी जल्द झुक सकती है।
बिहार में जातिगत सर्वे की सफलता और सियासी असर को देखते हुए अंततः मोदी सरकार ने कैबिनेट से जातिवार गिनती की मंजूरी दे दी।
🏛️ राजनीति की गर्माहट: कौन पक्ष में, कौन विरोध में
कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से लंबे समय से जाति जनगणना की मांग की जाती रही है। राहुल गांधी 2023 से लगातार हर मंच पर इसकी मांग दोहराते आए हैं। उनका तर्क रहा है कि “जनसंख्या के अनुपात में हक़” तभी संभव है जब जातिगत आंकड़े सामने आएं।
वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा –
“1947 से कांग्रेस ने जाति जनगणना का हमेशा विरोध किया। 2010 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इसे केवल विचार के स्तर पर छोड़ दिया।”
📈 क्यों जरूरी है जाति आधारित गणना?
- नीति निर्माण के लिए ठोस आंकड़े
आरक्षण, शिक्षा, नौकरियों में प्रतिनिधित्व जैसे मामलों में अक्सर “डाटा की कमी” बहस का विषय बनती रही है। जातीय जनगणना से यह शून्य भर सकता है। - मंडल कमीशन की विरासत
1979 में गठित मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में OBC आरक्षण लागू किया गया। लेकिन जातियों की सटीक संख्या आज भी अनौपचारिक अनुमानों पर आधारित है। - SC-ST-OBC की वास्तविक भागीदारी का आंकलन
2011 की जनगणना के अनुसार देश में SC आबादी 16.6% और ST आबादी 8.6% थी। OBC का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।
🗳️ राजनीतिक भूचाल और संभावित नफा-नुकसान
जातीय जनगणना कई राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है, खासकर उत्तर भारत में जहां OBC वोट बैंक निर्णायक है।
🔹 UP, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु जैसे राज्य जातीय जनगणना के बड़े समर्थक रहे हैं।
🔹 वहीं कुछ वर्गों में इस बात की आशंका भी है कि इससे जातिवाद और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है।
📜 क्या बदलेगा जनगणना फॉर्मेट?
2011 तक जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम होते थे। अब जातीय जनगणना को समायोजित करने के लिए इनमें अतिरिक्त कॉलम जोड़े जा सकते हैं, जिससे जाति, उपजाति, सामाजिक श्रेणी की जानकारी भी दर्ज की जा सके।
🧩 समाजशास्त्रियों और विपक्ष की नज़र में यह एक बड़ा मोड़
कई समाजशास्त्री इसे ‘न्यू सोशल जस्टिस मॉडल’ की ओर बढ़ता कदम मानते हैं। कांग्रेस, राजद, सपा, DMK, JDU और कई विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह आशंका भी जताई है कि सरकार “डेटा के नाम पर अधूरी तस्वीर” भी पेश कर सकती है।
🔚 निष्कर्ष:
भारत की जनसंख्या की असल सामाजिक रचना क्या है? कौन-सी जातियां किन हालात में हैं? और क्या मौजूदा नीतियां वास्तव में सब तक पहुँच रही हैं? — इन सभी सवालों के जवाब जातीय जनगणना 2026-27 से मिलने की उम्मीद है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है।